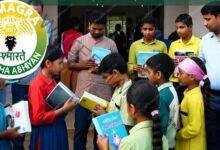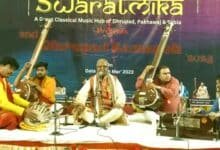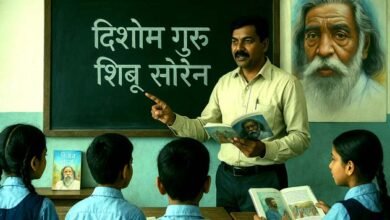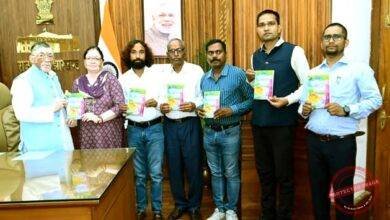रांची दर्पण डेस्क (मुकेश भारतीय)। Challenges of Jharkhand: भारत का झारखंड प्रदेश, जो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। अपनी अनूठी भौगौलिक विशेषताओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। जब इसे बिहार से अलग करके स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी रांची है। इसकी भौगौलिक स्थिति हरे-भरे जंगलों, पर्वत श्रृंखलाओं और नदियों से युक्त है, जो इसे एक प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र बनाती है। राज्य की प्रमुख नदियाँ स्वर्णरेखा, कोयल, दामोदर और गंगा की उपनदियाँ हैं।
झारखंड का ऐतिहासिक महत्व भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र आदिवासी समुदायों का प्रमुख केंद्र रहा है और यहाँ मुंडा, संथाल, उरांव और हो जैसे कई आदिवासी समूहों की प्रमुखता रही है। इन आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएँ हैं, जो झारखंड को एक विशिष्ट पहचान देती हैं। राज्य की सांस्कृतिक धरोहर में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों, कला रूपों और स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण योगदान है।
प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी झारखंड अत्यंत समृद्ध है। यह राज्य भारत के खनिज बैल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कोयला, लोहा, ताँबा, बॉक्साइट, कच्चा तेल और संगमरमर जैसे खनिजों का विशाल भंडार है, जो देश की औद्योगिक प्रगति में योगदान करते हैं। विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों की उपलब्धता ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सँभालने में मदद की है, बल्कि राष्ट्रीय औद्योगिक उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
झारखंड की जनसंख्या में बहुत विविधता पाई जाती है। यहाँ के मुख्य भाषाएँ हिंदी, संथाली, मुण्डारी और नागपुरी हैं। विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ के जनजीवन को विविध और रंगीन बनाते हैं, जिससे यह राज्य विविधता में एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है।
आर्थिक चुनौतियाँ
झारखंड प्रदेश की विकास यात्रा में कई आर्थिक चुनौतियाँ सामने आती हैं, जो विकास को बाधित करती हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति विकट है और यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानता जैसे मुद्दे प्रचलित हैं। इन समस्याओं के कारण झारखंड की जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में भी रुकावटें आती हैं।
गरीबी झारखंड की प्रमुख आर्थिक चुनौतियों में से एक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गंभीर है, जहां पर्याप्त रोजगार के अभाव में लोग अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गरीबी के इस चक्र से बाहर निकलने के लिए, समर्पित सरकारी योजनाओं और नीतियों की आवश्यकता है जो स्थायी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकें।
बेरोजगारी भी झारखंड की एक प्रमुख आर्थिक समस्या है। उच्च शिक्षित युवाओं से लेकर कम पढ़े-लिखे कामगारों तक, सभी वर्गों में बेरोजगारी दर चिंताजनक स्तर पर है। यह बेरोजगारी न केवल व्यक्तिगत स्तर पर विपत्तियों का कारण है, बल्कि समग्र आर्थिक विकास पर भी दुष्प्रभाव डालती है। सरकार ने रोजगार सृजन के विभिन्न प्रयास किए हैं। पर यह प्रयास अपेक्षित परिणाम देने में असफल रहे हैं।
क्षेत्रीय असमानता भी झारखंड के विकास में एक बड़ी बाधा है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विकास की गति और स्तर में भारी भिन्नता देखने को मिलती है। राजधानी रांची और कुछ अन्य बड़े शहरों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं का विकास तो देखा जाता है, लेकिन ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में यह अनुपस्थित है। इस असमानता को पाटने के लिए, दूरदराज के क्षेत्रों में भी बुनियादी ढांचे का विकास और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
शिक्षा और साक्षरता
झारखंड प्रदेश में शिक्षा प्रणाली की स्थिति वर्तमान में अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, जो राज्य के विकास में बड़ी बाधा बन रही है। सबसे पहली बात करें तो साक्षरता दर झारखंड में अपेक्षाकृत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल साक्षरता दर 66.41 प्रतिशत थी, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस साक्षरता दर में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है।
शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। प्राथमिक स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की कमी, शैक्षिक सामग्री की अनुपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों के चलते छात्रों की संख्या दिन-ब-दिन घटती जा रही है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित जैसे विषयों में विशेष शिक्षकों की अनुपस्थिति एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है।
आदिवासी और अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच और भी कठिन हो जाती है। इन इलाकों में स्कूलों की संख्या कम है और जो स्कूल हैं, वे भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इसका सीधा असर वहां के बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर पड़ता है। इसके अलावा, लड़कियों की शिक्षा दर भी चिंताजनक है। कई सामाजिक और आर्थिक कारणों से लड़कियों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, जिससे राज्य की कुल साक्षरता दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में असमानताओं को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने कई पहल की हैं। जैसे कि ‘सर्व शिक्षा अभियान’ और ‘मिड-डे मील योजना’। लेकिन ये पहलें अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई हैं। आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रथाएं और संरचनात्मक समस्याएँ राज्य के शिक्षा क्षेत्र को और भी जटिल बना देती हैं। इन्हें संबोधित किए बिना झारखंड प्रदेश में समग्र विकास की कल्पना करना कठिन है।
स्वास्थ्य सेवाएँ और सुविधाएँ
झारखंड प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में कई गंभीर खामियाँ हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की स्पष्ट असमानता एक प्रमुख समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अत्यंत सीमित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी, चिकित्सा उपकरणों की अनुपलब्धता और चिकित्सकों की भी कमी स्वास्थ्य सेवाओं के निरपेक्ष वितरण को प्रभावित करती है।
झारखंड के ग्रामीण हिस्सों में स्वास्थ्य जागरूकता का भी अभाव है। उचित जानकारी और संसाधनों की कमी के चलते लोग समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा स्टाफ का अभाव और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर रूप धारण कर लेती है।
शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अधिक विकट है। शहरी क्षेत्रों में भी विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती। स्वास्थ्य बजट की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित बजट आवश्यकताओं के विपरीत कम होता है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार में बाधा आती है।
बजटीय सीमाओं के कारण जरूरी चिकित्सा उपकरण और दवाएं समय पर नहीं मिल पातीं, और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता। इससे जनता को आपातकालीन स्थिति में बड़े स्वास्थ्य संकटों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के समाधान के बिना झारखंड में स्वस्थ समाज का निर्माण कठिन बना रहेगा।
भ्रष्टाचार और प्रशासनिक बाधाएँ
झारखंड प्रदेश के विकास में जिस बुनियादी समस्या ने व्यापक असर डाला है, वह है प्रशासनिक भ्रष्टाचार और नीति निर्माण में असंगठित निर्णय प्रक्रिया। विभिन्न स्तरों पर प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार ने न केवल राज्य की आर्थिक प्रगति में अवरोध पैदा किया है, बल्कि आम जनता का विश्वास भी हिला है। निम्न स्तर से उच्च प्रशासनिक पदों तक भ्रष्टाचार ने राज्य की विकास योजनाओं को प्रभावित किया है। इसका प्रत्यक्ष असर झारखंड के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं पर भी पड़ा है।
सरकारी अनुबंधों में भ्रष्टाचार, धन की हेराफेरी और मनमाने निर्णय प्रशासन की कार्यक्षमता को कमजोर करते हैं। जब नीति निर्माता अपने निजी स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं, तब आम जनता की जरूरतों की अनदेखी होती है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार ने न सिर्फ चिकित्सकीय सुविधाओं की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता को भी बाधित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का सीधा असर छात्रों की शैक्षिक गुणवत्ता पर पड़ता है, जो प्रदेश के दीर्घकालिक विकास पर भीआवरोधक का कार्य करता है।
भ्रष्टाचार का आर्थिक प्रभाव भी गहन होता है। विकास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण बजट का दुरुपयोग होता है, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी और गुणवत्ता में कमी आती है। इसके परिणामस्वरूप राज्य को अधिक लागत का सामना करना पड़ता है और जनता को मिलने वाली सुविधाओं में भी कटौती होने लगती है। यह स्थिति सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को भी प्रभावित करती है, जिससे आम लोगों में असंतोष और निराशा बढ़ती है।
इस प्रकार झारखंड प्रदेश के विकास में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक बाधाएँ प्रमुख अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें निष्प्रभावी बनाने के लिए नीति निर्माताओं और समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करना होगा।
झारखंड प्रदेश में पर्यावरणीय समस्याएँ विकास की राह में प्रमुख चुनौती साबित हो रही हैं। विशेष रूप से प्रदूषण, वनोन्मूलन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना क्षेत्र को करना पड़ रहा है। ये मुद्दे न केवल पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन पर भी गहरा असर डाल रहे हैं।
प्रदूषण
झारखंड में औद्योगिक और खनन गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर प्रदूषण पैदा कर रही हैं। यहाँ की नदियाँ, वायु और मृदा प्रचंड रूप से दूषित हो चुकी हैं। वायु प्रदूषण के कारण संक्रामक रोगों का प्रसार बढ़ गया है, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जल संसाधनों में भी भारी मात्रा में रासायनिक और विषैले पदार्थों का प्रवेश हो रहा है, जो कृषि और पेयजल गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहे हैं।
वनोन्मूलन
झारखंड के वनों की कटाई ने भी बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ावा दिया है। वनोन्मूलन के कारण जैवविविधता को हानि हो रही है और अनेक पशु-पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव और बाढ़ की समस्या भी बढ़ गई है। वन संरक्षण के प्रयासों की कमी तथा अवैध लकड़ी कटाई इस चुनौती को और भी जटिल बना रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन
स्थानीय जलवायु यहाँ के कृषि उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव डाल रही है। असामान्य वर्षा और सूखे के कारण फसल उत्पादन घट रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र में असंतुलित मौसमी घटनाओं की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप वातावरणिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई है।
समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय और राज्य सरकार को मिलकर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रदूषण नियंत्रण, वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सतत और सशक्त नीतियों का निर्माण आवश्यक है। जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय को समस्याओं के प्रति संवेदनशील और समाधान के प्रति सक्रिय बनाना होगा।
सामाजिक असमानता और जातिगत विभाजन
झारखंड प्रदेश का विकास एक अहम विषय रहा है, लेकिन इसकी प्रगति में सामाजिक असमानता और जातिगत विभाजन एक मुख्य बाधा प्रस्तुत करते हैं। जातिगत विभाजन और सामाजिक असमानता के कारण आर्थिक और शैक्षिक विकास में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न हुए हैं। ये विभाजन नस्ल, जाति और आर्थिक स्थिति के आधार पर साफ दिखाई देते हैं, जिससे समाज में विभिन्न वर्गों के बीच व्यापक खाई बनी हुई है।
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो झारखंड क्षेत्र में जनजातीय समुदायों का अलगाव हमेशा से एक जटिल समस्या रहा है। उपनिवेशी काल में ब्रिटिश शासन ने अपने आर्थिक और प्रशासनिक हितों के लिए समाज में विभाजन को और बढ़ावा दिया। जिसका प्रभाव आज तक निरंतर देखा जा सकता है। आजादी के बाद भी यह समस्या झारखंड के विकास के मार्ग में एक स्थायी बाधा के रूप में बनी हुई है।
आधुनिक संदर्भ में सामाजिक असमानता राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बड़ी समस्या है। क्षेत्रीय और स्थानीय शासन में इसकी झलक स्पष्ट है जहां नीति निर्धारण और कार्यान्वयन में विभिन्न वर्गों के प्रति असमान दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, पायली और गरीब वर्गों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समान रूप से नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में जातिगत विभाजन और भी गहरा होता जाता है।
वर्तमान में सामाजिक असमानता के कारण आर्थिक अवसर, शिक्षा और स्वास्थ सेवाओं में भारी असंतुलन बना हुआ है। यह असंतुलन न केवल परिवारिक और सामाजिक स्तर पर बल्कि राज्य की समग्र प्रगति में भी रुकावट पैदा कर रहा है। विकासशील योजनाओं में समावेश और निष्पक्ष नीति निर्धारण की आवश्यकता है, जिससे समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर मिल सकें।
समाधानों की दिशा में कदम
झारखंड प्रदेश के विकास में अब तक की बाधाओं को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार, सामाजिक संगठन और समुदाय मिलकर ठोस और कारगर उपाय अपनाएं। सरकारी नीतियों में बदलाव और बेहतर कार्यान्वयन आवश्यक है। सबसे पहले, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार की जरूरत है। इससे युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और राज्य का मानव संसाधन मजबूत बनेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हुए, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराना जरूरी है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज सेवी संगठनों को भी इस दिशा में आगे आकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ उठा सकें।
सामाजिक संगठनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गैर-सरकारी संस्थानों को विशेष परियोजनाओं पर कार्य करना चाहिए जैसे कि स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण परियोजनाएं। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। यह न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करेगा।
सामुदायिक भागीदारी भी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक है। सरकार को विभिन्न योजनाओं और नीतियों में स्थानीय लोगों की सलाह और सुझाव को शामिल करना चाहिए। क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, जहां लोग अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे प्रशासन के साथ साझा कर सकें। इस प्रकार, सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ाकर विकास को नया आयाम दिया जा सकता है।
- लोकसभा चुनाव छठा चरणः मतदानकर्मियों को बूथों तक जल्द पहुंचाने का निर्देश, जानें बड़ी वजह
- कल्पना सोरेन ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा- अब भाजपा…
- पूर्वी सिंहभूभ बना हॉट सीट, गीता कोड़ा को चुनौती देगी जोबा मांझी
- सांसद संजय सेठ का प्रयास रंग लाया, 150 टन का कचरा संधारण प्लांट तैयार
- मोरहाबादी मैदान में होगा राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का भव्य आयोजन, 785 जनजातीय समुदाय का होगा जमावड़ा
[web_stories title=”true” excerpt=”false” author=”true” date=”false” archive_link=”true” archive_link_label=”” circle_size=”150″ sharp_corners=”false” image_alignment=”left” number_of_columns=”1″ number_of_stories=”4″ order=”DESC” orderby=”post_date” view=”carousel” /]